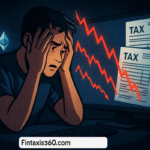भाग 1: भारतीय आयकर कानून की आधारशिला
1.1 परिचय: आयकर अधिनियम, 1961 और नियम, 1962 का अवलोकन
भारत में आयकर का ढाँचा मुख्य रूप से आयकर अधिनियम, 1961 (Income Tax Act, 1961) द्वारा शासित होता है, जो 1 अप्रैल, 1962 से प्रभावी हुआ । यह एक व्यापक कानून है जिसमें 298 धाराएँ और 14 अनुसूचियाँ शामिल हैं, जो भारत में कराधान के विभिन्न पहलुओं को परिभाषित करती हैं । यह अधिनियम वह मूल कानून है जो आय पर कर लगाने, कर की दरों को निर्धारित करने, और कर संग्रह की प्रक्रिया को रेखांकित करता है।
इस अधिनियम के प्रावधानों को व्यावहारिक रूप से लागू करने के लिए, आयकर नियम, 1962 (Income Tax Rules, 1962) बनाए गए हैं । इन नियमों को बनाने का अधिकार केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes – CBDT) को है, जो भारत में प्रत्यक्ष करों के प्रशासन के लिए शीर्ष निकाय है । यह कानूनी संरचना एक जानबूझकर किया गया द्विविभाजन है, जहाँ अधिनियम ‘मूल कानून’ (substantive law) स्थापित करता है और नियम ‘प्रक्रियात्मक कानून’ (procedural law) प्रदान करते हैं। इस पृथक्करण से प्रणाली में लचीलापन आता है। संसद प्रमुख नीतिगत बदलावों के लिए वित्त अधिनियम के माध्यम से अधिनियम में संशोधन करती है, जबकि CBDT प्रक्रियात्मक समायोजन के लिए नियमों में संशोधन कर सकता है, जिससे प्रणाली को निरंतर विधायी हस्तक्षेप के बिना अधिक अनुकूलनीय बनाया जा सकता है ।
1.2 महत्वपूर्ण परिभाषाएं: कर अनुपालन की भाषा को समझना
आयकर कानून को समझने के लिए कुछ मौलिक अवधारणाओं को जानना आवश्यक है:
- वित्तीय वर्ष (Financial Year – FY): यह 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाली 12 महीने की अवधि है। इस अवधि के दौरान आय अर्जित की जाती है ।
- निर्धारण वर्ष (Assessment Year – AY): यह वित्तीय वर्ष के ठीक बाद की 12 महीने की अवधि है, जो 1 अप्रैल से शुरू होती है। इस वर्ष में, पिछले वित्तीय वर्ष में अर्जित आय का आकलन किया जाता है और उस पर कर लगाया जाता है। उदाहरण के लिए, 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 (FY 2024-25) के दौरान अर्जित आय का निर्धारण वर्ष 2025-26 (AY 2025-26) होगा ।
- करदाता (Assessee): कोई भी व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF), कंपनी, फर्म या अन्य इकाई जो आयकर अधिनियम के तहत कर या कोई अन्य राशि (जैसे ब्याज या जुर्माना) का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।
- आय के पाँच शीर्षक (Five Heads of Income): अधिनियम के तहत, कर योग्य आय की गणना के लिए सभी स्रोतों से होने वाली आय को पाँच मुख्य शीर्षकों में वर्गीकृत किया गया है:
- वेतन से आय (Income from Salaries)
- गृह संपत्ति से आय (Income from House Property)
- व्यवसाय या पेशे से लाभ और अभिलाभ (Profits and Gains of Business or Profession)
- पूंजीगत लाभ (Capital Gains)
- अन्य स्रोतों से आय (Income from Other Sources) यह वर्गीकरण महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक शीर्षक के तहत आय की गणना और अनुमत कटौतियों के लिए विशिष्ट नियम हैं ।
1.3 भारत में कराधान का ढाँचा
- प्रत्यक्ष कर (Direct Tax): आयकर एक प्रत्यक्ष कर है, जिसका अर्थ है कि इसका भार उसी व्यक्ति द्वारा वहन किया जाता है जिस पर यह लगाया जाता है। इसे किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है ।
- आधिकारिक पोर्टल: आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट
incometaxindia.gov.inऔर ई-फाइलिंग पोर्टलincometax.gov.inसभी नवीनतम सूचनाओं, नियमों, परिपत्रों और ऑनलाइन सेवाओं जैसे कि आयकर विवरणी (ITR) दाखिल करने और कर भुगतान के लिए प्राथमिक और सबसे विश्वसनीय स्रोत हैं ।
भाग 2: कर व्यवस्थाओं का विस्तृत विश्लेषण: पुरानी बनाम नई
भारतीय करदाताओं के पास वर्तमान में अपनी कर देयता की गणना के लिए दो व्यवस्थाओं के बीच चयन करने का विकल्प है। यह निर्णय किसी व्यक्ति की वित्तीय योजना और कर बचत पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है।
2.1 दोनों व्यवस्थाओं का मौलिक अंतर
- पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime): यह पारंपरिक व्यवस्था है जो अपेक्षाकृत उच्च कर दरों की पेशकश करती है, लेकिन करदाताओं को आयकर अधिनियम के विभिन्न वर्गों के तहत लगभग 70 प्रकार की कटौतियों और छूटों का दावा करने की अनुमति देती है। इनमें धारा 80C (निवेश), 80D (स्वास्थ्य बीमा), मकान किराया भत्ता (HRA), और गृह ऋण पर ब्याज जैसी लोकप्रिय कटौतियाँ शामिल हैं ।
- नई कर व्यवस्था (New Tax Regime): इसे एक सरलीकृत विकल्प के रूप में पेश किया गया है जिसमें कम कर दरें हैं, लेकिन यह अधिकांश कटौतियों और छूटों को समाप्त कर देती है । इसका मुख्य उद्देश्य कर फाइलिंग प्रक्रिया को आसान बनाना और उन करदाताओं को लाभ पहुंचाना है जो कर-बचत योजनाओं में निवेश नहीं करते हैं।
2.2 डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था: एक महत्वपूर्ण बदलाव
निर्धारण वर्ष 2024-25 से, नई कर व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट विकल्प बना दिया गया है । इसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई करदाता आयकर विवरणी दाखिल करते समय सक्रिय रूप से पुरानी व्यवस्था का चयन नहीं करता है, तो उनकी कर गणना स्वचालित रूप से नई व्यवस्था के तहत की जाएगी। वेतनभोगी व्यक्ति हर साल अपनी सुविधा के अनुसार दोनों व्यवस्थाओं के बीच स्विच कर सकते हैं, लेकिन व्यवसाय या पेशे से आय वाले व्यक्तियों के लिए यह विकल्प सीमित है; एक बार नई व्यवस्था से बाहर निकलने के बाद, वे केवल एक बार ही वापस आ सकते हैं ।
यह एक तटस्थ विकल्प नहीं है, बल्कि एक सुविचारित नीतिगत कदम है। सरकार सक्रिय रूप से एक विकल्प को अधिक आकर्षक और अपनाने में आसान बना रही है। इस “नज” नीति का उद्देश्य दो गुना हो सकता है: पहला, सरकार के लिए कर प्रशासन को सरल बनाना, क्योंकि इससे विभिन्न प्रकार की जटिल कटौतियों के सत्यापन की आवश्यकता कम हो जाती है। दूसरा, आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए कर अनुपालन को सरल बनाना, जिससे संभावित रूप से कर आधार का विस्तार हो सकता है। इस नीति का एक अप्रत्यक्ष लेकिन महत्वपूर्ण परिणाम घरेलू बचत की आदतों में बदलाव हो सकता है। दशकों से, कर नीति ने धारा 80C के तहत विशिष्ट साधनों (जैसे PPF, बीमा, ELSS) में बचत को प्रोत्साहित किया है। इन कटौतियों को कम प्रासंगिक बनाकर, सरकार अप्रत्यक्ष रूप से इन लॉक-इन बचत साधनों से अधिक तरल बाजार निवेश या यहाँ तक कि उच्च खपत की ओर एक बदलाव को प्रोत्साहित कर सकती है, जिसके महत्वपूर्ण व्यापक आर्थिक प्रभाव हो सकते हैं।
2.3 आपके लिए कौन सी व्यवस्था बेहतर है: एक निर्णय-निर्धारण ढाँचा
सही कर व्यवस्था का चुनाव पूरी तरह से आपकी आय, निवेश और वित्तीय लक्ष्यों पर निर्भर करता है।
- पुरानी व्यवस्था कब चुनें: यह व्यवस्था उन व्यक्तियों के लिए अत्यधिक फायदेमंद है जो महत्वपूर्ण कटौतियों का दावा कर सकते हैं। यदि आपके पास गृह ऋण है और आप ब्याज पर बड़ी राशि का भुगतान कर रहे हैं (धारा 24 के तहत ₹2 लाख तक), आप HRA छूट का दावा करते हैं, और आप धारा 80C (₹1.5 लाख) और 80D (स्वास्थ्य बीमा) के तहत पूरी तरह से निवेश करते हैं, तो पुरानी व्यवस्था आपकी कर योग्य आय को काफी कम कर सकती है । एक विशेषज्ञ विश्लेषण के अनुसार, यदि आपकी कुल योग्य कटौतियाँ ₹4 लाख या उससे अधिक हैं, तो पुरानी व्यवस्था लगभग हमेशा बेहतर विकल्प होगी ।
- नई व्यवस्था कब चुनें: यह उन करदाताओं के लिए आदर्श है जिनके पास दावा करने के लिए बहुत कम या कोई कटौती नहीं है। यदि आप किराए के घर में नहीं रहते हैं, कोई गृह ऋण नहीं है, और कर-बचत योजनाओं में बहुत अधिक निवेश नहीं करते हैं, तो नई व्यवस्था की कम दरें सीधे तौर पर फायदेमंद होंगी ।
तालिका 1: पुरानी बनाम नई कर व्यवस्था – एक तुलनात्मक अवलोकन (AY 2025-26 और AY 2026-27)
| विशेषता (Feature) | पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) | नई कर व्यवस्था (New Tax Regime – AY 2025-26) | नई कर व्यवस्था (New Tax Regime – AY 2026-27) |
| डिफ़ॉल्ट स्थिति | नहीं | हाँ | हाँ |
| मूल छूट सीमा (60 वर्ष से कम) | ₹2,50,000 | ₹3,00,000 | ₹4,00,000 |
| मानक कटौती (वेतनभोगी) | ₹50,000 | ₹50,000 | ₹75,000 |
| धारा 87A के तहत छूट | ₹5 लाख तक की आय पर ₹12,500 | ₹7 लाख तक की आय पर ₹25,000 | ₹12 लाख तक की आय पर ₹60,000 |
| धारा 80C/80D/HRA की उपलब्धता | हाँ | नहीं (कुछ अपवादों को छोड़कर) | नहीं (कुछ अपवादों को छोड़कर) |
| वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाभ | उच्च मूल छूट सीमा | कोई अतिरिक्त लाभ नहीं | कोई अतिरिक्त लाभ नहीं |
Export to Sheets
भाग 3: आकलन वर्ष 2025-26 और 2026-27 के लिए आयकर स्लैब और दरें

3.1 पुरानी कर व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब (AY 2025-26)
पुरानी कर व्यवस्था के तहत स्लैब दरें अपरिवर्तित बनी हुई हैं और करदाता की आयु के अनुसार भिन्न होती हैं ।
तालिका 2: व्यक्ति (60 वर्ष से कम) और HUF के लिए स्लैब
| आय स्लैब | कर दर |
| ₹2,50,000 तक | शून्य |
| ₹2,50,001 से ₹5,00,000 | 5% |
| ₹5,00,001 से ₹10,00,000 | 20% |
| ₹10,00,000 से अधिक | 30% |
Export to Sheets
तालिका 3: वरिष्ठ नागरिक (60-80 वर्ष) के लिए स्लैब
| आय स्लैब | कर दर |
| ₹3,00,000 तक | शून्य |
| ₹3,00,001 से ₹5,00,000 | 5% |
| ₹5,00,001 से ₹10,00,000 | 20% |
| ₹10,00,000 से अधिक | 30% |
Export to Sheets
तालिका 4: अति वरिष्ठ नागरिक (80 वर्ष से अधिक) के लिए स्लैब
| आय स्लैब | कर दर |
| ₹5,00,000 तक | शून्य |
| ₹5,00,001 से ₹10,00,000 | 20% |
| ₹10,00,000 से अधिक | 30% |
Export to Sheets
3.2 नई कर व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब (AY 2025-26)
वित्तीय वर्ष 2024-25 (AY 2025-26) के लिए, नई कर व्यवस्था के तहत स्लैब दरें सभी व्यक्तियों के लिए समान हैं, चाहे उनकी आयु कुछ भी हो ।
तालिका 5: सभी व्यक्तियों के लिए लागू दरें (AY 2025-26)
| आय स्लैब | कर दर |
| ₹3,00,000 तक | शून्य |
| ₹3,00,001 से ₹7,00,000 | 5% |
| ₹7,00,001 से ₹10,00,000 | 10% |
| ₹10,00,001 से ₹12,00,000 | 15% |
| ₹12,00,001 से ₹15,00,000 | 20% |
| ₹15,00,000 से अधिक | 30% |
3.3 बजट 2025 के बाद: नई कर व्यवस्था के संशोधित स्लैब (AY 2026-27 से प्रभावी)
बजट 2025 में नई कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की गई, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 (AY 2026-27) से लागू होंगे। इन बदलावों का उद्देश्य मध्यम वर्ग को राहत देना और नई व्यवस्था को और अधिक आकर्षक बनाना है।
- मूल छूट सीमा: मूल छूट सीमा को ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹4 लाख कर दिया गया है ।
- संशोधित स्लैब: कर स्लैब को पुनर्गठित किया गया है, जिसमें 30% की उच्चतम दर अब ₹15 लाख के बजाय ₹24 लाख से अधिक की आय पर लागू होगी ।
नई कर व्यवस्था में यह पुनर्गठन विशेष रूप से मध्य और उच्च-मध्यम आय वर्ग (₹12 लाख से ₹24 लाख) को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पुरानी “नई व्यवस्था” के तहत, ₹20 लाख कमाने वाले व्यक्ति को ₹15 लाख से ऊपर की आय पर 30% की दर से कर देना पड़ता था। संशोधित संरचना के तहत, वे उसी आय के विभिन्न हिस्सों पर 15%, 20% और 25% की कम दरों पर कर का भुगतान करेंगे। यह इस आय समूह के लिए एक सीधी कर कटौती है और नई व्यवस्था को उन लोगों के लिए लगभग सार्वभौमिक रूप से बेहतर बनाती है जिनके पास मध्यम कटौती है।
तालिका 6: संशोधित नई कर व्यवस्था स्लैब (AY 2026-27)
| आय स्लैब | कर दर |
| ₹4,00,000 तक | शून्य |
| ₹4,00,001 से ₹8,00,000 | 5% |
| ₹8,00,001 से ₹12,00,000 | 10% |
| ₹12,00,001 से ₹16,00,000 | 15% |
| ₹16,00,001 से ₹20,00,000 | 20% |
| ₹20,00,001 से ₹24,00,000 | 25% |
| ₹24,00,000 से अधिक | 30% |
भाग 4: प्रमुख कटौतियाँ और छूट (मुख्यतः पुरानी व्यवस्था के तहत)
पुरानी कर व्यवस्था का मुख्य आकर्षण विभिन्न कटौतियों और छूटों का लाभ उठाने की क्षमता है, जो कर योग्य आय को काफी कम कर सकती हैं।
4.1 धारा 80C: सबसे लोकप्रिय कर-बचत उपकरण
यह धारा करदाताओं को एक वित्तीय वर्ष में ₹1.5 लाख तक की कटौती का दावा करने की अनुमति देती है। यह कटौती केवल पुरानी कर व्यवस्था में उपलब्ध है । इसके तहत कुछ प्रमुख निवेश विकल्प हैं:
- कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF)
- जीवन बीमा प्रीमियम (LIC)
- इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS)
- राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC)
- 5-वर्षीय कर-बचत सावधि जमा
- बच्चों की ट्यूशन फीस
4.2 धारा 80D: स्वास्थ्य सुरक्षा पर कर लाभ
यह धारा स्वयं, जीवनसाथी, बच्चों और माता-पिता के लिए भुगतान किए गए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कटौती प्रदान करती है। 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए सीमा ₹25,000 है, जबकि वरिष्ठ नागरिक माता-पिता के लिए अतिरिक्त ₹50,000 तक की कटौती का दावा किया जा सकता है ।
4.3 वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए भत्ते
- मकान किराया भत्ता (HRA): वेतनभोगी व्यक्ति जो किराए के आवास में रहते हैं, कुछ शर्तों के अधीन प्राप्त HRA पर छूट का दावा कर सकते हैं। यह केवल पुरानी व्यवस्था में उपलब्ध है ।
- अवकाश यात्रा भत्ता (LTA): कर्मचारी घरेलू यात्रा पर किए गए खर्चों के लिए LTA छूट का दावा कर सकते हैं, जो कुछ नियमों और शर्तों के अधीन है ।
4.4 गृह ऋण पर ब्याज (धारा 24(b))
पुरानी व्यवस्था के तहत, करदाता स्व-अधिकृत संपत्ति के लिए गृह ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज पर ₹2 लाख तक की कटौती का दावा कर सकते हैं ।
4.5 अन्य महत्वपूर्ण कटौतियाँ
- धारा 80E: उच्च शिक्षा ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज पर कटौती ।
- धारा 80TTA/80TTB: बचत खाते से ब्याज आय पर क्रमशः सामान्य व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कटौती ।
- NPS में अतिरिक्त निवेश (धारा 80CCD(1B)): धारा 80C की सीमा के अलावा, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में ₹50,000 तक के निवेश पर अतिरिक्त कटौती ।
तालिका 7: पुरानी कर व्यवस्था के तहत प्रमुख कटौतियों की सूची
| धारा (Section) | कटौती का विवरण (Description of Deduction) | अधिकतम सीमा (Maximum Limit) |
| मानक कटौती | वेतनभोगी और पेंशनभोगियों के लिए | ₹50,000 |
| 80C, 80CCC, 80CCD(1) | PPF, EPF, LIC, ELSS, NPS, आदि में निवेश | कुल मिलाकर ₹1,50,000 |
| 80CCD(1B) | NPS में अतिरिक्त योगदान | ₹50,000 |
| 80D | स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम | स्वयं/परिवार के लिए ₹25,000 (वरिष्ठ नागरिक के लिए ₹50,000) + माता-पिता के लिए अतिरिक्त |
| 24(b) | गृह ऋण पर ब्याज (स्व-अधिकृत संपत्ति) | ₹2,00,000 |
| HRA (धारा 10(13A)) | मकान किराया भत्ता | निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार गणना |
| 80E | शिक्षा ऋण पर ब्याज | भुगतान किया गया वास्तविक ब्याज (8 वर्षों तक) |
| 80TTA | बचत खाते पर ब्याज (वरिष्ठ नागरिकों को छोड़कर) | ₹10,000 |
| 80TTB | जमा पर ब्याज (वरिष्ठ नागरिकों के लिए) | ₹50,000 |
भाग 5: नई कर व्यवस्था के तहत विशेष प्रावधान (AY 2026-27 से प्रभावी)
बजट 2025 ने नई कर व्यवस्था को वेतनभोगी करदाताओं के लिए कहीं अधिक आकर्षक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव पेश किए, जो AY 2026-27 से लागू होंगे।
5.1 धारा 87A के तहत बढ़ी हुई छूट: ₹12 लाख तक की आय पर शून्य कर
AY 2026-27 से लागू होने वाला सबसे बड़ा बदलाव धारा 87A के तहत कर छूट (Rebate) में वृद्धि है। छूट की राशि को ₹25,000 से बढ़ाकर ₹60,000 कर दिया गया है ।
इस प्रावधान का प्रभाव यह है कि जिन व्यक्तियों की कुल कर योग्य आय ₹12 लाख तक है, उन्हें कोई आयकर नहीं देना होगा। गणना इस प्रकार काम करती है:
- ₹4 लाख तक की आय पर कर: ₹0
- ₹4 लाख से ₹8 लाख तक की आय पर (अगले ₹4 लाख पर 5%): ₹20,000
- ₹8 लाख से ₹12 लाख तक की आय पर (अगले ₹4 लाख पर 10%): ₹40,000
- कुल कर देयता: ₹20,000 + ₹40,000 = ₹60,000
- धारा 87A के तहत छूट: -₹60,000
- अंतिम देय कर: शून्य
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह एक छूट (Rebate) है, न कि छूट सीमा (Exemption Limit)। इसका मतलब है कि ₹12 लाख से अधिक आय वाले व्यक्ति इस लाभ के पात्र नहीं होंगे और उन्हें अपनी पूरी कर योग्य आय पर लागू स्लैब दरों के अनुसार कर का भुगतान करना होगा।
5.2 मानक कटौती: वेतनभोगी और पेंशनभोगियों के लिए एक समान लाभ
AY 2026-27 से, नई कर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी व्यक्तियों और पेंशनभोगियों के लिए ₹75,000 की मानक कटौती (Standard Deduction) शुरू की गई है । यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इसने पुरानी व्यवस्था के एक प्रमुख लाभ को समाप्त कर दिया है। पहले, नई व्यवस्था में मानक कटौती की कमी वेतनभोगी करदाताओं के लिए इसे न अपनाने का एक बड़ा कारण थी। अब, नई व्यवस्था में एक
उच्च मानक कटौती (पुरानी व्यवस्था में ₹50,000 की तुलना में) शुरू करके, सरकार ने लाखों वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए निर्णय को सरल बना दिया है। इस कटौती के कारण, ₹12.75 लाख तक की सकल वेतन आय वाले व्यक्ति प्रभावी रूप से शून्य कर का भुगतान करेंगे (₹12.75 लाख – ₹75,000 = ₹12 लाख कर योग्य आय) ।
5.3 नई व्यवस्था में अनुमत सीमित कटौतियाँ
हालांकि अधिकांश कटौतियाँ समाप्त कर दी गई हैं, फिर भी कुछ चुनिंदा कटौतियाँ नई व्यवस्था के तहत उपलब्ध हैं, जिनमें शामिल हैं:
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) टियर-I खाते में नियोक्ता का योगदान (धारा 80CCD(2))।
- अग्निवीर कॉर्पस फंड में किया गया योगदान (धारा 80CCH) ।
भाग 6: विभिन्न स्रोतों से आय की गणना
6.1 वेतन से आय की गणना
वेतन से कर योग्य आय की गणना में सकल वेतन से कुछ कटौतियों को घटाना शामिल है।
- सकल वेतन की गणना: इसमें मूल वेतन, महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), अवकाश यात्रा भत्ता (LTA), और अन्य भत्ते और अनुलाभ (perquisites) शामिल हैं।
- कटौतियाँ: सकल वेतन से, मानक कटौती घटाई जाती है (पुरानी व्यवस्था में ₹50,000 और AY 2026-27 से नई व्यवस्था में ₹75,000) ।
- कर योग्य वेतन: कटौतियों के बाद बची हुई राशि ‘वेतन से आय’ होती है। नियोक्ता द्वारा जारी किया गया फॉर्म 16 वेतन, भत्तों और स्रोत पर कर कटौती (TDS) का एक विस्तृत विवरण प्रदान करता है ।
6.2 गृह संपत्ति से आय की गणना
गृह संपत्ति से आय की गणना एक चरण-दर-चरण प्रक्रिया है ।
- सकल वार्षिक मूल्य (Gross Annual Value – GAV) का निर्धारण: यह संपत्ति से अपेक्षित किराया है। इसकी गणना संपत्ति के उचित किराए, नगरपालिका मूल्यांकन और मानक किराए (यदि लागू हो) की तुलना करके की जाती है। किराए पर दी गई संपत्ति के लिए, GAV वास्तविक प्राप्त किराए या अपेक्षित किराए, जो भी अधिक हो, के बराबर होता है। स्व-अधिकृत संपत्ति के लिए GAV शून्य माना जाता है ।
- शुद्ध वार्षिक मूल्य (Net Annual Value – NAV) की गणना: GAV में से उस वित्तीय वर्ष के दौरान मालिक द्वारा भुगतान किए गए नगरपालिका करों (जैसे संपत्ति कर) को घटाकर NAV प्राप्त किया जाता है ।
- कटौतियों का दावा: NAV से दो कटौतियों की अनुमति है:
- मानक कटौती: NAV का 30% (मरम्मत और रखरखाव के लिए) ।
- गृह ऋण पर ब्याज (धारा 24(b)): संपत्ति की खरीद, निर्माण या मरम्मत के लिए लिए गए ऋण पर भुगतान किया गया वास्तविक ब्याज ।
- कर योग्य आय: इन कटौतियों के बाद बची हुई राशि ‘गृह संपत्ति से आय’ होती है।
6.3 पूंजीगत लाभ से आय की गणना
पूंजीगत संपत्ति (जैसे संपत्ति, शेयर, म्यूचुअल फंड) की बिक्री से होने वाले लाभ पर पूंजीगत लाभ कर लगता है।
- अल्पकालिक पूंजीगत लाभ (Short-Term Capital Gain – STCG): यह उन संपत्तियों की बिक्री पर होता है जिन्हें एक छोटी अवधि (आमतौर पर इक्विटी के लिए 12 महीने और संपत्ति के लिए 24 महीने) के लिए रखा जाता है। STCG पर सामान्य स्लैब दरों के अनुसार कर लगता है, सिवाय सूचीबद्ध इक्विटी/इक्विटी म्यूचुअल फंड के, जिन पर 20% की विशेष दर लागू होती है (बजट 2025 में 15% से बढ़ाई गई) ।
- दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (Long-Term Capital Gain – LTCG): यह उन संपत्तियों की बिक्री पर होता है जिन्हें निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रखा जाता है।
- इक्विटी और इक्विटी म्यूचुअल फंड: एक वित्तीय वर्ष में ₹1.25 लाख से अधिक के लाभ पर 12.5% की दर से कर लगता है, जिसमें इंडेक्सेशन का कोई लाभ नहीं होता है ।
- अन्य संपत्तियाँ (जैसे संपत्ति, ऋण म्यूचुअल फंड): इंडेक्सेशन के लाभ के साथ 20% की दर से कर लगता है ।
- लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (Cost Inflation Index – CII): इंडेक्सेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो मुद्रास्फीति के लिए संपत्ति की खरीद लागत को समायोजित करती है, जिससे कर योग्य लाभ कम हो जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए CII 363 है ।
भाग 7: अधिभार, उपकर और सीमांत राहत
7.1 अधिभार (Surcharge): उच्च आय पर अतिरिक्त कर
उच्च आय वाले करदाताओं को आयकर के ऊपर एक अतिरिक्त अधिभार का भुगतान करना पड़ता है। दरें आय के स्तर के आधार पर भिन्न होती हैं:
- ₹50 लाख से ₹1 करोड़ तक की आय पर: 10%
- ₹1 करोड़ से ₹2 करोड़ तक की आय पर: 15%
- ₹2 करोड़ से ₹5 करोड़ तक की आय पर: 25%
- ₹5 करोड़ से अधिक की आय पर: 37% (नोट: नई कर व्यवस्था में ₹2 करोड़ से अधिक की आय पर उच्चतम अधिभार दर 25% है) ।
एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि लाभांश आय और धारा 111A (STCG) और 112A (LTCG) के तहत पूंजीगत लाभ पर देय कर पर अधिभार की अधिकतम दर 15% तक सीमित है ।
7.2 स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर (Health and Education Cess)
सभी करदाताओं को देय आयकर और अधिभार (यदि लागू हो) की कुल राशि पर 4% की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर का भुगतान करना होता है ।
7.3 सीमांत राहत (Marginal Relief): एक सुरक्षा जाल
सीमांत राहत एक ऐसा तंत्र है जो यह सुनिश्चित करता है कि जब किसी व्यक्ति की आय एक अधिभार स्लैब से दूसरे में जाती है (जैसे ₹50 लाख या ₹1 करोड़ को पार करती है), तो देय अतिरिक्त कर आय में हुई वृद्धि से अधिक न हो। यह उन करदाताओं को अनुचित कर बोझ से बचाता है जिनकी आय इन सीमाओं से थोड़ी ही अधिक है ।
भाग 8: आयकर विवरणी (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तिथियाँ
8.1 सही ITR फॉर्म का चयन
सही ITR फॉर्म का चयन करना आपकी आय के स्रोतों पर निर्भर करता है:
- ITR-1 (सहज): उन निवासी व्यक्तियों के लिए जिनकी कुल आय ₹50 लाख तक है, और आय का स्रोत वेतन, एक गृह संपत्ति और अन्य स्रोत (जैसे ब्याज) हैं ।
- ITR-2: उन व्यक्तियों और HUF के लिए जिन्हें पूंजीगत लाभ से आय होती है या जिनके पास एक से अधिक गृह संपत्ति है ।
- ITR-3: उन व्यक्तियों और HUF के लिए जिन्हें व्यवसाय या पेशे से लाभ होता है ।
- ITR-4 (सुगम): उन व्यक्तियों, HUF और फर्मों के लिए जिनकी आय धारा 44AD, 44ADA या 44AE के तहत अनुमानित आधार पर गणना की जाती है ।
8.2 ITR दाखिल करने की प्रक्रिया
- लॉगिन: आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल (
incometax.gov.in) पर अपने पैन (उपयोगकर्ता आईडी) और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें । - ITR दाखिल करें: डैशबोर्ड पर, ‘ई-फाइल’ > ‘आयकर रिटर्न’ > ‘आयकर रिटर्न दाखिल करें’ पर क्लिक करें ।
- विवरण चुनें: निर्धारण वर्ष (जैसे 2025-26), फाइलिंग का तरीका (‘ऑनलाइन’), और अपनी स्थिति (जैसे ‘व्यक्तिगत’) चुनें।
- ITR फॉर्म चुनें: अपनी आय प्रोफ़ाइल के आधार पर सही ITR फॉर्म चुनें।
- डेटा भरें: फॉर्म में पहले से भरा हुआ डेटा (pre-filled data) होता है। इसे अपने दस्तावेजों (जैसे फॉर्म 16, बैंक विवरण) से सत्यापित करें और आवश्यक सुधार करें।
- सत्यापन और जमा करें: सभी अनुसूचियों को भरने और कर की गणना की पुष्टि करने के बाद, अपनी विवरणी को ई-सत्यापित करें। ई-सत्यापन आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किया जा सकता है।
8.3 आकलन वर्ष 2025-26 के लिए महत्वपूर्ण तिथियाँ
AY 2025-26 के लिए ITR उपयोगिता फॉर्म जारी करने में देरी और बाद में समय सीमा के विस्तार ने करदाताओं और पेशेवरों के लिए एक आवर्ती चुनौती को उजागर किया है। यह एक कुशल डिजिटल शासन के नीतिगत लक्ष्य और जमीनी हकीकत के बीच एक कार्यान्वयन अंतर को इंगित करता है। ITR-2 और ITR-3 जैसी जटिल विवरणियों के लिए उपयोगिताओं को जारी करने में 100-दिन की देरी जैसी घटनाएं करदाताओं के लिए अनिश्चितता पैदा करती हैं और सटीक फाइलिंग के लिए उपलब्ध समय को कम करती हैं।
तालिका 8: आकलन वर्ष 2025-26 के लिए महत्वपूर्ण कर तिथियाँ
| गतिविधि (Activity) | नियत तिथि (Due Date) |
| ITR फाइलिंग की शुरुआत | 30 मई, 2025 |
| अग्रिम कर की पहली किस्त | 15 जून, 2025 |
| ITR फाइलिंग (गैर-ऑडिट मामले) | 15 सितंबर, 2025 (31 जुलाई से विस्तारित) |
| अग्रिम कर की दूसरी किस्त | 15 सितंबर, 2025 |
| ITR फाइलिंग (ऑडिट मामले) | 31 अक्टूबर, 2025 |
| अग्रिम कर की तीसरी किस्त | 15 दिसंबर, 2025 |
| विलंबित/संशोधित विवरणी दाखिल करना | 31 दिसंबर, 2025 |
| अग्रिम कर की चौथी किस्त | 15 मार्च, 2026 |
भाग 9: रणनीतिक कर योजना और विशेषज्ञ सिफारिशें
प्रभावी कर योजना का अर्थ है अपनी आय और निवेश को इस तरह से व्यवस्थित करना ताकि आपकी कर देयता को कानूनी रूप से कम किया जा सके।
- तुलनात्मक विश्लेषण: कर दाखिल करने से पहले, हमेशा अपनी अनुमानित आय और कटौतियों के आधार पर पुरानी और नई दोनों व्यवस्थाओं के तहत अपनी कर देयता की गणना करें। ऑनलाइन आयकर कैलकुलेटर इस प्रक्रिया को सरल बना सकते हैं।
- जीवन स्तर के अनुसार योजना:
- युवा वेतनभोगी: यदि आपके पास कोई बड़ी कटौती नहीं है, तो नई व्यवस्था (विशेषकर AY 2026-27 से) लगभग हमेशा फायदेमंद होगी।
- गृह ऋण वाला परिवार: यदि आपका गृह ऋण ब्याज और 80C निवेश मिलाकर ₹4 लाख से अधिक है, तो पुरानी व्यवस्था आपके लिए बेहतर हो सकती है।
- सेवानिवृत्ति के करीब: यदि आपकी आय मुख्य रूप से पेंशन और ब्याज से है, और आपके पास वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा है, तो दोनों व्यवस्थाओं की सावधानीपूर्वक तुलना करें।
- निवेश का समय: यदि आप पुरानी व्यवस्था चुन रहे हैं, तो वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही अपने कर-बचत निवेश (जैसे ELSS SIP, PPF) की योजना बनाएं ताकि अंतिम समय की हड़बड़ी से बचा जा सके।
- आम गलतियों से बचें:
- अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें। उपयोगिता में देरी और पोर्टल पर अंतिम समय में होने वाली भीड़ से बचने के लिए जल्दी फाइल करें।
- अपनी सभी आय, जिसमें बचत खाते का ब्याज, सावधि जमा का ब्याज और लाभांश शामिल हैं, की रिपोर्ट करना सुनिश्चित करें।
- सही ITR फॉर्म चुनें। गलत फॉर्म का उपयोग करने से आपकी विवरणी ‘दोषपूर्ण’ हो सकती है।
भाग 10: निष्कर्ष
वित्तीय वर्ष 2025-26 (निर्धारण वर्ष 2026-27) के लिए आयकर नियम भारत के कर परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक हैं। सरकार का झुकाव स्पष्ट रूप से नई, सरलीकृत कर व्यवस्था की ओर है, जैसा कि बढ़ी हुई छूट सीमा, उच्च मानक कटौती और पुनर्गठित कर स्लैब से स्पष्ट है। ये परिवर्तन नई व्यवस्था को, विशेष रूप से ₹12.75 लाख तक की आय वाले वेतनभोगी करदाताओं के लिए, एक अत्यंत आकर्षक विकल्प बनाते हैं।
हालांकि, पुरानी कर व्यवस्था उन लोगों के लिए प्रासंगिक बनी हुई है जो गृह ऋण, HRA और विभिन्न निवेशों के माध्यम से महत्वपूर्ण कटौतियों का लाभ उठाते हैं। अंतिम निर्णय व्यक्तिगत वित्तीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। करदाताओं के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपनी आय और संभावित कटौतियों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करें और दोनों व्यवस्थाओं के तहत अपनी कर देयता की गणना करें। समय पर अनुपालन, सही ITR फॉर्म का चयन, और सूचित निर्णय लेना न केवल कानूनी आवश्यकता है, बल्कि एक विवेकपूर्ण वित्तीय रणनीति भी है। जैसे-जैसे कर कानून विकसित हो रहे हैं, सूचित और सक्रिय रहना ही अपनी कर-दक्षता को अधिकतम करने की कुंजी है।
Discover more from Finance and Taxation
Subscribe to get the latest posts sent to your email.